10th Class Hindi Vyakaran Notes Question Answer Guide Summery Extract Mcq Pdf Download in Kannada Medium Karnataka State Syllabus 2025 दसवीं कक्षा हिंदी व्याकरण नोट्स हिंदी व्याकरण pdf हिन्दी व्याकरण class 10 state syllabus sslc hindi vyakaran notes pdf class 10 hindi grammar notes pdf download हिंदी व्याकरण हिंदी व्याकरण class 10 syllabus Class 10 Book 10ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ ವ್ಯಾಕರಣ ನೋಟ್ಸ್ 10th Hindi Notes Pdf
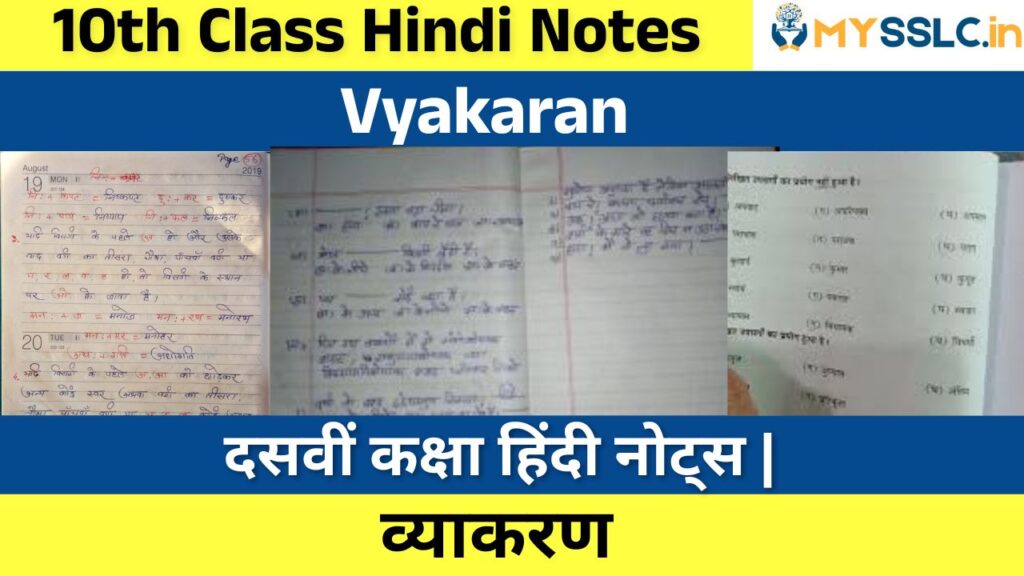
1.प्रेरणार्थक क्रिया
क्रिया का वह रूप जिससे कर्ता खुद कार्य नहीं करके, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं।
उदा :
- राम पढ़ता है। (क्रिया)
- राम पढ़ाता है। (प्रेरणार्थक क्रिया)
प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप मिलते हैं।
- प्रथम प्रेरणार्थक रूप
- द्वितीय प्रेरणार्थक रूप
उदा :
- राम जी ने पढ़ा। (क्रिया)
- रामजी ने छात्रों को पढ़ाया। (प्रथम प्रेरणार्थक)
- रामजी ने छात्रों को श्याम से पढ़वाया। (द्वितीय प्रेरणार्थक)
प्रेरणार्थक क्रियाओं के कुछ उदाहरण
| क्रिया | प्रथम प्रेरणार्थक रूप | द्वितीय प्रेरणार्थक रूप |
| पढ़ना | पढ़ाना | पढ़वाना |
| करना | कराना | करवाना |
धातु के अंत में दीर्घ स्वर हो तो उसे हस्व मे बदलकर प्रेरणार्थक रूप बना सकते हैं ।
उदा :
| धातु | क्रिया | प्र.प्रे. रूप | द्वि.प्रे. रूप |
| जाग | जागना | जगाना | जगवाना |
| जीत | जीतना | जिताना | जितवाना |
2.संधि
‘संधि’ शब्द का अर्थ है मेल। दो वर्षों अथवा अक्षरों के मेल से होनेवाले परिवर्तन या बदलाव की संधि कहते हैं ।
उदा :
जन + अधिकार = जनाधिकार (अ+ अ आ)
जन + आदेश = जनादेश (अ आ आ)
संधि के तीन भेद है:
- स्वर संधि
- व्यंजन संधि
- विसर्ग संधि
1. स्वर संधि
जब दो स्वर आपस में मिलकर एक नया रूप ले लेते हैं, तब उसे स्वर-संधि कहते हैं। स्वर संधि के पाँच भेद हैं
- दीर्घ संधि
- गुण संधि
- वृद्धि संघि
- यण संधि
- अयादि संधि
दीर्घ संधि
दो सवर्णों के मिलने से दीर्घ हो जाता है। यदि अ, आ, इ, ई, उ, ऊ और ऋ के बाद वे ही हस्व या दीर्घ स्वर आयें, तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, ऊ और ऋ हो जाते हैं।
क) अ+ अ = आ समान + अधिकार = समानाधिकार
अ + आ = आ पुण्य + आत्मा = पुण्यात्मा
आ + अ आ शिक्षा + अर्थी = शिक्षार्थी
आ + अ आ विद्या + आलय = विद्यालय
ख) इ + इ = ई रवि + इन्द्र = रवीन्द्र
इ + ई = ई गिरि + ईश = गिरीश
ई + इ = ई मही + ईश = महीश
ई + ई = ई रजनी + ईश = रजनीश
ग) उ + उ = ऊ लघु + उत्तर = लघुत्तर
उ + ऊ = ऊ सिंधु ऊर्मि= सिंधूर्मि
ऊ+ उ = ऊ वधू + उत्सव = वधूसतवा
ऊ + ऊ = ऊ भू + ऊर्जा = भूर्जा
घ) ऋ + ऋ = ऋ पितृ +ऋण = पितृण
गुण संधि
यदि अया आआ के बाद इया उयाऊ और ऋ आये तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओर और अर हो जाते हैं ।
उदाहरण :
क) अ + ड = ए गज + इंद् = गजेंद्र
अ + ई = ए परम + ईश्वर = परमेश्वर
आ + इ = ए महा + इन्दु = महेन्दु
आ + ई = ए महा + ईश = महेश
ख) अ +उ =ओ राम + उत्सव = रामोत्सव
अ + ऊ = ओ जल + ऊर्मि = जलोर्मि
आ + उ =ओ महा + उदय = महोदय
आ + ऊ = ओ महा + ऊर्मि = महोर्मि
ग) अ + ऋ = अर सप्त + ऋषि = सप्तर्षि
आ + ऋ = अर महा + ऋषि = महर्षि
वृद्धि संधि
यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आये तो दोनों के स्थान में ऐ तथा अ या आ के बाद ओ या और आये तो दोनों के स्थान में औ हो जाता है।
क) अ + ए = ऐ एक + एक = एकैक
अ + ऐ = ऐ मत + ऐक्य = मतैक्य
आ + ए =ऐ सदा + एव = सदैव
आ + ऐ = ऐ महा + ऐश्वर्य = महैश्वर्य
अ +ओ = औ परम + ओज = परमौज
अ + औ = औ वन + औषध = वनौषध
आ + औ = औ महा + औजस्वी = महौजस्वी
यदि इ, ई, उ, ऊ और ऋ के बाद कोई भिन्न स्वर आये तो इ-ई का यू, उऊ का व् और ऋ का र हो जाता है।
उदा :
इ + अ = य अति अंत्य = अत्यंत
इ + आ = या इति + आदि = इत्यादि
इ+ अ = यु प्रति + उपकार = प्रत्युपकार
उ+ अं = व मनु + अंतर = मन्वंतर
ऋ + अ = र पितृ + अनुमति = पित्रानुमति
ऋ + आ = र पितृ + आज्ञा = पित्राज्ञा
ऋ + उ = र पितृ + उपदेश = पितृपदेश
अयादि संधि
यदि ए, ऐ और ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय ऐ का आय, ओ का अन् और औ का ओव हो जाता है।
उदा :
(क) ए + अ = अय चे + अन = चयन
ए + अ = अय ने + अन = नयन
(ख) ऐ + अ = आय गै + अक = गायक
ऐ + इ = आय नै + इका = नायिका
(ग) ओ + अ = अव भो + अन = भवन
औ + अ = आव पौ + अन = पावन
(य) औ + इ = आव नौ + इक = नाविक
2 व्यंजन संधि
व्यंजन के स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को व्यंजन संधि करते हैं।
उदा :
- दिक् + गज = दिग्गज
- सत् + वाणी = सद्वाणी
- अच् + अंत = अजंत
- षट् + दर्शन = षड्दर्शन
- वाक् + जाल = वाग्जाल
- तत् + रूप = तद्रूप
3. विसर्ग संधि
स्वरों अथवा व्यंजनों के साथ विसर्ग (:) के मेल से विसर्ग में जो बदलाव होता है, उसे विस्वर्ण संधि कहते हैं।
उदा :
निः चय = निश्चय
निः + रस = नीरस
दुः + गंध = दुर्गंध
मनः + रघ = मनोरथ
पुरः + हित = पुरोहित
3. समास
दो भिन्न शब्दों के मिलन से विशिष्ट अर्थ का बोध कराने वाले पदसमुदाय को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलन से बननेवाला शब्द ‘समस्त पद’ कहलाता है। समस्त पद को अलग करने के विधान को विग्रहवाक्य कहते हैं।
समास के छः भेद होते हैं:
- कर्मधारय समास
- द्विगु समास
- बहुव्रीहि समास
- तत्पुरुष समास
- द्वंद्व समास
- अत्ययीभाव समास
1.कर्मधारय समास
समास का पहला शब्द पूर्व पद कहलाता है तो आखिरी शब्द उत्तर पद कहलाता है । दोनों शब्दों में एक शब्द की उपमा दूसरे से की जाती है।
उदा:
क) पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष्य
| पहला पद | दूसरा पद | समस्त पद | विग्रह |
| पीत | अंबर | पीतांबर | पीत है जो अंबर |
| नील | आकाश | नीलाकाश | आकाश जो नीला है |
ख) पहला पद उपमान और दूसरा उपमेय
उदा:
| कनक | लता | कनकलता | कनक के समान लता |
| चन्द्र | मुख | चन्द्रमुख | चन्द्र के समान मुख |
ग) पहला पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान
उदा:
| मुख | चंद्र | मुखचंद्र | चाँद रूपी मुख |
| चरण | कमल | चरणकमल | कमल रूपी चरण |
2.तत्पुरुष समास
विस समास में उत्तर पद (दूसरा पद) प्रधान हो, वह तत्पुरुष समास कहलाता है।
जैसे : ग्रंथकार – ग्रंथ को लिखनेवाला
तुलसीकृत – तुलसी के द्वारा कृत
देशप्रेम – देश के लिए प्रेम
देशनिकाला – देश से निकाला
3. द्विगु समास
जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो. उसे द्विगु समास कहते है।
उदा: त्रिमूर्ति, सप्तऋषि, नवग्रह
4. द्वंद्व समास
जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, उसे द्वन्द्व समास कहते हैं ।
उदा: रामलक्ष्मण = राम और लक्ष्मण
शिवपार्वती = शिव और पार्वती
5. बहुव्रीहि समास
जिस समास में पूर्व और उत्तर पदों की प्रधानता न होकर, किसी अन्य पद की प्रमुखता हो तो उसे बह समास कहते हैं।
उदा :
त्रिनेत्र = जिसके तीन नेत्र हो शंकर
चतुर्भुज = जिसकी चार भुजाएँ हो – विष्णु
गजवदन = जिसका वदन हाथी का मुख जैसा हो – गणेश
6.अव्ययीभाव समास
जिस समास में पहला पद अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं।
उदा: यथावत्, आकंठ, भरपेट
4. एकल शब्द
अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का प्रयोग
एक वाक्य या वाक्यांश के बदले एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता हो, उसे एकल शब्द कहते हैं
उदा :
निर्धन – जिसके पास धन न हो
कवि – जो कविता लिखता हो
गायक – जो गीत गाता हो
5. मुहावरे
जिस वाक्यांश से प्रकट अर्थ से अलग अर्थ का बोध हो, उसे मुहावरा कहते हैं ।
उदा : दिल पिघलना – दया दिखाना
छाती चौड़ा होना – बहुत खुश होना, गर्व करना
6. कहावतें
जिस कथन में गहरा और मूल्यवान अर्थ हो उस वाक्य को कहावत या लोकोक्ति कहते हैं ।
उदा : अधजल गगरी छलकत जाय ।
कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर
चार दिन की चाँदनी ।
7. विराम चिन्ह
जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं, उन्हें विराम चिहन कहते हैं। ये निम्न प्रकार है।
- अल्प विराम (,)
- अर्ध विराम (;)
- पूर्ण विराम (1)
- प्रश्न चिह्न (?)
- विस्मयादिबोधक (!)
- योजक चिह्न (-)
- उद्दरण चिह्न (“”)
- कोष्टक चिह्न ( )
- विवरण चिह्न (: -) (:)
8. काल
क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता हो, उसे काल कहते हैं । काल के तीन भेद है।
- भूतकाल
- वर्तमान काल
- भविष्यत् काल
1.भूतकाल :
क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि काम बीते समय में हो चुका था या हो रहा था, उसे भूतकाल कहते हैं ।
उदा : राम ने खाना खाया ।
श्याम ने किताब पढ़ी ।
उमा रोटी खा चुकी है।
रेखा बाज़ार गई है।
2. वर्तमान काल
क्रिया के जिस रूप से यह मालूम हो कि काम अभी हो रहा हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं।
उदा : शंकर पढ़ता है, पार्वती पढ़ रही है।
भविष्यत् काल :
क्रिया के जिस रूप से यह पता चलते हैं कि काम अभी होना बाकी है अर्थात आगे आनेवाले समय होगा, उसे भविष्यत् काल कहते हैं।
जैसे: मैं कल बेंगलूरू जाऊँगा ।
अध्याषक पाठ पढ़ायेगा ।
शायद वह कल आ जाए ।
9. लिंग
संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में दो प्रकार के लिंग हैं-
- पुल्लिग
- स्त्रीलिंग
1.पुल्लिंग: पुरुष जाति का बोध करानेवाले शब्द पुल्लिंग होते हैं ।
जैसे – आदमी, बेटा, कुत्ता आदि।
2.स्त्रीलिंग: स्त्री जाति का बोध करानेवाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं।
जैसे – लड़की, औरत, माँ आदि।
पुल्लिंग अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग की पहचान के कुछ सूत्र इस प्रकार हैं一
1. प्रायः बड़ी, भारी और मोटी वस्तुओं के शब्द पुल्लिग होते हैं।
जैसे – थैला, डिब्बा, थाल आदि।
2. पर्वत, देश, समुद्र, पेड़, अनाज, वार, मास, ग्रह-नक्षत्र, समय, धातु, द्रव, रत्न के नाम पुल्लिग होते हैं।
3.अक, अन, आर, एरा, त्व, ना, आपा, आव, पन आदि प्रत्यय से बननेवाले शब्द पुल्लिग होते हैं। जैसे तैराक, पवन, सुनार, लुटेरा, मनुष्यत्व, रोना, मोटापा, बचाव, लड़कपन आदि।
4. प्रायः प्राणीवाचक शब्दों में स्त्री जाति को बतानेवाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं।
जैसे बहन, पत्नी, बेटी आदि।
5. नदी, झील, भाषा, बोली, लिपि, कुछ नक्षत्र, तिथि, तारीख । शरीर के ये अंग आँख, नाक, कमर, छाती, जीभ, पलक, कोहनी, कलाई खाने की चीजें रोटी, कचौड़ी, पूरी, दाल, सब्जी; संस्कृत के आकारांत, उकारांत और इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं।
6.आवट, आहट, आई, आस, इमा, नी आदि प्रत्यय से बननेवाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं।
जैसे- बनावट, मुस्कराहट, पढ़ाई, कपास, मधुरिमा , करनी आदि ।
इन सूत्रों की सहायता से स्त्रीलिंग और पल्लिग शब्दों को पहचाना जा सकता है तथा विभिन्न प्रत्ययों को जोड़कर लिंग रूप बना सकते हैं।
पुल्लिग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम :
1. अ को आ करके
पुल्लिंग – स्त्रीलिंग
- छात्र – छात्रा
- आचार्य – आचार्या
2.अ. आ को ई करके
पुल्लिंग – स्त्रीलिंग
- नर – नारी
- नाना – नानी
3.आ को इया करके
पुल्लिंग – स्त्रीलिंग
- कुत्ता – कुतिया
- बेटा – बिटिया
4.शब्दों के अंत में अ, ई के स्थान पर इन जोड़कर
पुल्लिंग – स्त्रीलिंग
- सुनार – सुनारिन
- नाई – नाइन
5.शब्दों के अंत में अ, आ, ई, उ, ए के स्थान
पुल्लिंग – स्त्रीलिंग
- ठाकुर – ठकुराइन
- ठकुराइन – हलवाइन
6.अक को इका बनाकर
पुल्लिंग – स्त्रीलिंग
- बालक – बालिका
- सेवक – सेविका
7.शब्द के अंत में आनी जोड़कर
पुल्लिंग – स्त्रीलिंग
- सेठ – सेठानी
- नौकर – नौकरानी
8.अकारांत शब्दों के अंत में नी जोड़कर
पुल्लिंग – स्त्रीलिंग
- शेर – शेरनी
- मोर – मोरनी
9.आन का अती के रूप में बदलकर
पुल्लिंग – स्त्रीलिंग
- महान – महती
- श्रीमान – श्रीमती
- भाग्यवान – भाग्यवती
10. ई के स्थान पर इनी लगाकर
पुल्लिंग – स्त्रीलिंग
- स्वामी – स्वमिनी
- एकाकी – एकाकिनी
11.ता के स्थान पर त्री लगाकर
पुल्लिंग – स्त्रीलिंग
- दाता – दात्री
- विधाता – विधात्री
12.कुछ विशेष शब्द जिनका स्त्रीलिंग में भिन्त्र रूप हो जाता है-
पुल्लिंग – स्त्रीलिंग
- भाई – बहन
- नर – मादा
10. कारक
संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है, उसे कहते हैं ।
उदा :
1.रामय्या ने सुब्बय्या को एक पुस्तक दी।
2.फिलिफ ने महमूद की एक तस्वीर खींची ।
कारक के आठ भेद होते हैं।
1.कर्ताकारक : इससे क्रिया करनेवाले का बोध होता है। इसका विभक्ति चिन्ह है -‘ने’
उदा : 1. सदाशिव ने खाना खाया ।
2.सावित्री ने पानी पिया ।
2.कर्मकारक : इससे क्रिया के फल भोगनेवाले का पता चलता है। इसका चिन्ह है – ‘को’ ।
उदा : पुलिस ने चोर को पकड़ लिया
अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया ।
3.करण कारक: इससे क्रिया के होन में सहायता देनेवाले साधन का बोध होता है। इस कारक का चिह्न है – ‘से’।
उदा: सुमा कलम से लिखती है।
दासय्या कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है।
4. संप्रदान कारक: इससे क्रिया करने के उद्देश्य या आशय का पता चलता है। इस कारक का चिह्न हैं के लिए, के द्वारा, के वास्ते
उदा: सुब्बय्या ने अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर साड़ी खरीदी ।
विनीत ने अपनी बहिन के वास्ते एक खूबसूरत थैली खरीदी ।
5. अपादान कारक : इससे किसी किया के एक स्थान से हटने या दूर होने का बोध होता है। इस कारक का चिह्न है – ‘से’
उदा : गंगा हिमालय से निकलती है।
शेर गुफा से निकलता है।
6. संबंध कारक: इससे संज्ञाओं के बीच भिन्न-भिन्न प्रकार के संबंध का बोध होता है। इस कारक के चिह्न हैं का, के, क
उदा : कुएँ का पानी स्वच्छ होता है।
रामय्या के पिता किसान हैं।
उदा : ममता की माँ हिन्दी पढ़ाती है।
7.अधिकरण कारक: इससे क्रिया के होने के स्थान या समय का बोध होता है। इस कारक के चिह्न है – ‘में’ और ‘पर’
उदा : पेड़ पर चीता बैठता है।
8. संबोधन कारक: इससे किसी संज्ञा को पुकारने का भाव प्रकट होता है। इस कारक के चिह्न हैं – अरे, हे, ओ, इत्यादि ।
उदा : अरे ! तुम यह क्या कर रहे हो?
हे राम ! यह क्या हो गया।
10.’कि’ और ‘की’ का प्रयोग
‘कि’ कारण बोधक अव्यय है। कार्य कारण वाचक अव्यय के रूप में उन वाक्यों के आरंभ में इसका प्रयोग होता है।
उदा :
राम ने कहा कि लक्ष्मण तुम घर लौटो ।
श्याम बाहर जानेवाला था कि उसके पिताजी दफ्तर से लौटे।
‘कि’ अव्यय के प्रयोग से वाक्यार्थ में विकल्प का बोध होता है।
जैसे
- तुम नौकरी करोगे कि व्यापार ?
- सीता गई कि गीता ?
‘की’ का प्रयोग
स्त्री लिंग एक वचन और बहुवचन सूचक संज्ञा शब्दों के संबंध बताने के लिए ‘की’ का प्रयोग होता है।
जैसे : 1.कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू है।
2. मैसूर की लड़कियाँ ।
- घर की रोटियाँ ।
- शिवानी की किताबें ।
(ख) ‘की’ का प्रयोग भूतकालिक क्रिया के रूप में भी होता है।
जैसे: महती ने परीक्षा पास की ।
नील वेंकट ने चार धाम की यात्रा की।
उसने किसी की बुराई नहीं की।
(ग) ‘की’ का प्रयोग संबंधबोधक अव्यय के एक अंग के रूप में भी होता है।
जैसे : तिरुपति की ओर ।
गुरूजी की तरफ ।
सिंह की भाँति ।
11.विरुद्धार्थक शब्द
एक दूसरे के ठीक विरोध प्रकट करनेवाले शब्दों का विरुद्धार्थक या विरोधवाचक शब्द कहते हैं । इन्हें ‘विलोम’ शब्द के नाम से पुकारते हैं।
विरुद्धार्थक शब्दों की रचना (हीन इत्यादि) और उपसर्ग (कु, सु, दु, नि, अ, अन, अप आदि की मदद से होती है। कभी-कभी स्वतंत्र शब्द भी वितेधवाचक होते हैं।
(क) कुछ लोकप्रिय विरुद्धार्थक शब्द :
- माता X पिता
- शेर X शेरनी
- आगे X पीछे
- आय X व्यय
- बैल X गाय
(ख) उपसर्ग जोड़कर तथा उपसर्ग में बदलाव के द्वारा भी विपरीतार्थक शब्द बनाये जाते हैं।
जैसे :
- जय X पराजय
- कीर्ति X अपकीर्ति
- सफल X असफल
(ग)’अ’ तथा ‘अन’ के जोड़ने के द्वारा भी विरुद्धार्थक शब्द बनते हैं ।
जैसे:
- आदर X अनादर
- स्वीकार अस्वीकार
- लिखित X अलिखित
- आवश्यक X अनावश्यक
